विचार
हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर यह सोचने का भी दिन, आईने पर हम कितनी धूल, कालिख लगा चुके हैं!
हिन्दी पत्रकारिता दिवस (30 मई) अपनी विभूतियों के प्रति न सिर्फ कृतज्ञता ज्ञापन, बल्कि यह सोचने का भी दिन है कि उनके दिए आईने पर हम कितनी धूल, कालिख लगा चुके हैं।
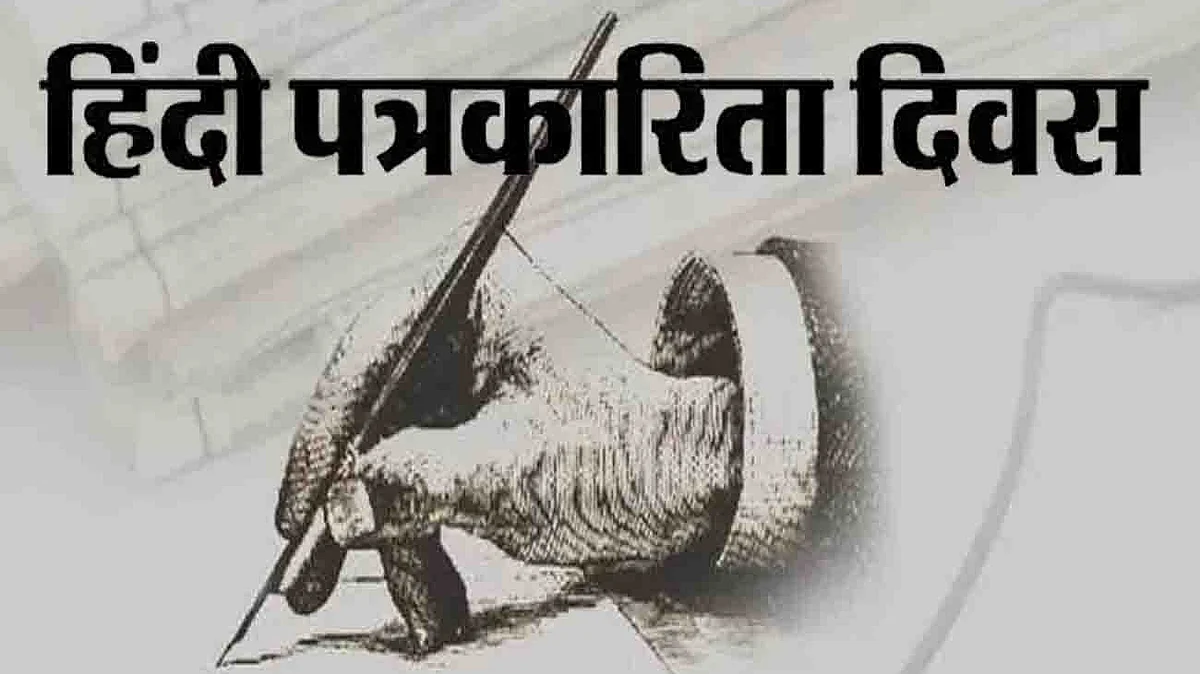
हिन्दी की पत्रकारिता और उसके साहित्य का संबंध इतना अन्योन्याश्रित रहा है कि कहा जाता है कि पत्रकारिता के पास तोप से मुकाबले वाला बहुप्रचारित हौसला साहित्य की मार्फत ही आया। तब, जब गोरी सत्ता के एक के बाद एक प्रायः सारी हदें पार करती जाने के दौर में मशहूर उर्दू साहित्यकार अकबर इलाहाबादी ने लिखा- ‘खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।’
यों, अखबारों की शक्ति में ऐसा विश्वास जताने वाले अकबर इलाहाबादी अकेली शख्सियत नहीं हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा ही है कि चार विरोधी अखबारों की मारक क्षमता के आगे हजारों बंदूकों की ताकत बेकार हो जाती है। मैथ्यू आर्नाल्ड की मानें तो पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य ही है, क्योंकि जैसे साहित्य भावों का भरोसा हुआ करता है, पत्रकारिता तथ्यों का भरोसा हुआ करती है।
Published: undefined
एक समय हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के प्रायः सारे संपादक या तो साहित्यकार हुआ करते थे या हिन्दी भाषा के बडे़ ज्ञाता। आजादी की लड़ाई के दौरान जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने और खुद उसकी आवाज सुन पाने के लिए महात्मा गांधी समेत कई जननेताओं ने भी पत्रकारिता और संपादनकर्म को अपना हथियार बनाया। लेकिन वह साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिभाओं की निर्बाध व स्वाभाविक आवाजाही से सर्वथा अलग मामला था।
मिसालों पर जाएं तो आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह और भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चन्द्र से शुरू कर महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह ‘दिनकर’, बालकृष्ण शर्मा नवीन से लेकर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती, राजेन्द्र माथुर और प्रभाष जोशी तक की सुदीर्घ परंपरा हमारे सामने है।
Published: undefined
लेकिन आज न सिर्फ साहित्य और पत्रकारिता के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है (कहना चाहिए, बढ़ाई जा रही है), बल्कि उन्हें एक दूजे का विलोम माना जाने लगा है। इस तरह कि अनेक मीडिया संस्थानों के संपादकीय विभागों में साहित्यकारों का ‘अकाल’ है। अपनी-अपनी कोटरियों में ‘कैद’ पत्रकार और साहित्यकार कई बार दो ऐसे ध्रुवों या छोरों पर बैठे दिखाई देते हैं, जहां उनमें सृजनात्मक संवाद और मेल-मिलाप की कतई कोई गुंजायश ही नहीं दिखाई देती। क्या आश्चर्य कि हिन्दी पत्रकारिता-प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व डिजिटल- सब में साहित्य की जगहें सिकुड़ती जा रही हैं। दूसरी ओर साहित्य में तो पत्रकारिता जैसे हो ही नहीं रही।
सभी जानते हैं कि इससे हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता- दोनों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई मुंह नहीं खोलता कि इससे ‘आप-आप ही’ वाली जिस ‘संस्कृति’ का ‘निर्माण’ हो रहा है, उसका लाभार्थी कौन है? वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी के इस कथन की मार्फत जवाब तक पहुंचा जा सकता है कि ‘साहित्य अकेला और निहत्था हो गया है: उसे बुद्धि-ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रों से समर्थन और सहचारिता नहीं मिल पा रहे हैं।’ निस्संदेह, साहित्य के बगैर पत्रकारिता निहत्थी भले न हुई हो, अकेली तो वह भी हो ही गई है। उसके कई स्वनामधन्य हस्ताक्षरों के धत्कर्मों से तो लगता है कि वह पत्रकारिता ही नहीं रह गई है। मीडिया नाम उसे यों ही तो रास नहीं आने लगा है।
Published: undefined
दूसरे पहलू पर जाएं तो हिन्दी भाषा, खासतौर पर उसके शब्दों व पत्रकारिता (वह साहित्यिक हो, सामाजिक या राजनीतिक) का अब तक जो भी संस्कार या मानकीकरण संभव हो पाया है (दूसरे शब्दों में कहें तो उनके स्वरूप में जो स्थिरता आई है), वह कोई एक दिन या कुछ समय की कोशिशों से ही संभव नहीं हुआ है। उस सबके पीछे एक समय उसके उन्नयन की अगुआई में अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले स्वाभिमानी संपादकों की जज्बे व जिदों से भरी अहर्निश सेवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
यह बड़ी भूमिका हिन्दी पत्रकारिता के ‘शिल्पकार’ और ‘भीष्म पितामह’ कहलाने वाले मराठीभाषी बाबूराव विष्णु पराड़कर (16 नवंबर 1883-12 जनवरी 1955) से बहुत पहले से दिखाई देने लगती है, लेकिन उसे ठीक से रेखांकित उन्हीं के समय से किया जाता है। दरअसल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिन्दी पत्रकारिता को जनजागरण का अस्त्र बनाकर विदेशी सत्ताधीशों की नाक में दम करने और स्वतंत्रता के बाद नए भारत के निर्माण के लिए प्रयुक्त करने में उन्होंने खुद को ऐसा क्रांतिकारी शब्दशिल्पी तो बनाया ही, जिसके एक हाथ में कलम और दूसरे में पिस्तौल हुआ करती थी, अप्रतिम संपादकाचार्य भी बनाया। नहीं बनाया होता तो उनके वक्त स्थिरीकरण व मानकीकरण के दौर से गुजर रही हिन्दी भाषा और पत्रकारिता अनेक ऐसे शब्दों (साथ ही संपादकों से) वंचित रह जाती, जिनके बगैर आज वह काम नहीं चला पाती।
Published: undefined
साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें तो अपने वक्त की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका ‘सरस्वती’ के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी (09 मई 1864 - 21 दिसंबर, 1938) की उसे उत्कृष्ट बनाए रखने की जिद यहां तक थी कि कहते हैं, एक सज्जन ने उसके लिए उन्हें अपनी कविताएं भेजीं और अरसे तक उनके न छपने पर याद दिलाया कि ‘मैं वही हूं, जिसने एक बार आपको गंगा में डूबने से बचाया था’, तो आचार्य द्विवेदी का जवाब था: आप चाहें तो मुझे ले चलिए, गंगा में वहीं फिर से डुबो दीजिए, जहां आपने डूबने से बचाया था, लेकिन मैं ये कविताएं ‘सरस्वती’ में नहीं छाप सकता।’ जो मैथिलीशरण गुप्त अब राष्ट्रकवि कहलाते हैं, एक समय उनकी कविताएं उन्होंने यह कहकर छापने से मना कर दी थीं कि ‘सरस्वती’ खड़ी बोली की पत्रिका है और वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। इसके बाद गुप्त ने उन्हें खड़ी बोली की कविताएं भेजीं, लेकिन अपना ब्रजभाषा वाला रसिकेन्द्र नाम ही लिखा, तो भी उन्हें फटकार ही मिली: ‘रसिकेन्द्र का जमाना चला गया’। फिर आचार्य ने उन्हें पत्र लिखा- आप ‘सरस्वती’ में लिखना चाहें तो इधर-उधर अपनी रचनाएं छपाने का विचार छोड़ दीजिए। जिस कविता को हम चाहें, उसे छापेंगे। लेकिन जिसे न चाहें, उसे भी न कहीं दूसरी जगह छपाइए, न किसी को दिखाइए, ताले में बंद करके रखिए। अपना लिखा सभी को अच्छा लगता है परंतु उसके अच्छे-बुरे का विचार दूसरे लोग ही कर सकते हैं।’ उनकी यह जिद ‘रसिकेन्द्र’ को मैथिलीशरण गुप्त बनाकर ही तुष्ट हुई।
अलबत्ता, ‘अस्थिरता’ के बदले ‘अनस्थिरता’ शब्द के पक्ष में बालमुकुन्द गुप्त से हुए लंबे विवाद में पूरी शक्ति लगाकर भी आचार्य न उसका औचित्य सिद्ध कर पाए, न ही उसे प्रचलन में ला पाए। लेकिन ‘सरस्वती’, ‘भारतमित्र’ और ‘हिन्दी बंगवासी’ आदि पत्रिकाओं में उसको लेकर चले लंबे विवाद से इतना तो हुआ ही कि लेखक और संपादक भाषा और वर्तनी की एकरूपता व व्याकरणसम्मतता के प्रति पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे।
Published: undefined
उन्हीं की ‘सरस्वती’ से निकले गणेशशंकर विद्यार्थी (26 अक्तूबर 1890- 25 मार्च 1931) अपने द्वारा संपादित ‘प्रताप’ के मुखपृष्ठ पर उसके मास्टहेड के ठीक नीचे उनका रचा यह दोहा छापते थे: ‘जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है’। विद्यार्थी का जज्बा ऐसा था कि उन्होंने ‘प्रताप’ के प्रवेशांक में घोषणा की थी: ‘समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को समझते हैं।’ उनकी संपादकीय नैतिकता के तमाम उदाहरण हैं।
‘विशाल भारत’ के बहुचर्चित संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी (24 दिसंबर 1892- 2 मई 1985) की वृत्ति और भी स्वतंत्र व विशिष्ट थी। उनके प्रायः सारे संपादकीय फैसलों की एक ही कसौटी थी: क्या उससे देश, समाज उसकी भाषाओं और साहित्यों, खासकर हिन्दी का कुछ भला होगा या मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी या नहीं। और जिद तो उनकी ऐसी थी कि उन्होंने छायावाद और सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ के विरुद्ध अभियान शुरू किया तो उससे साहित्य जगत में उठे तूफान के बावजूद टस से मस होना स्वीकार नहीं किया।
यहां उल्लिखित संपादक ‘बटलोई के चावल’ भर हैं और हिन्दी भाषा व पत्रकारिता अपने उन्नयन के लिए ऐसे और भी कितने ही समर्पित संपादकों की जिद और जज्बे की कर्जदार है। हिन्दी पत्रकारिता दिवस सच पूछिए तो उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। यह सोचने का भी कि उनके दिए आईने पर हम कितनी धूल, कालिख और खरोंचे देखने को अभिशप्त हो चले हैं?
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined